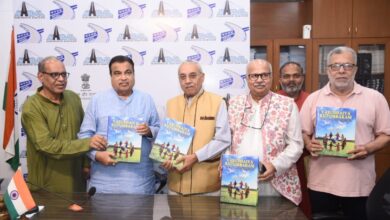विजय गर्ग
विश्व मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, इस साल वायुमंडल का औसत तापमान औद्योगिकीकरण से पहले के तापमान की तुलना में 1.54 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है. ग्लोबल वार्मिंग के कारणों की जांच करने और इसे रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1996 से आयोजित किया जा रहा है। 2015 के पेरिस शिखर सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए सभी संभव उपाय करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बंद कर दिया गयायदि नहीं, तो 2028 तक तापमान 1.5 डिग्री से अधिक हो जाएगा, जिसके बाद सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से निपटना और तापमान वृद्धि को रोकना और अधिक कठिन हो जाएगा। सदस्य देशों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयास किये हैं, लेकिन तापमान वृद्धि की गति से पता चलता है कि वे अपर्याप्त रहे हैं।
अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में केवल दो उल्लेखनीय समझौते हो सके। पहला कार्बन क्रेडिट योजना पर था, जो लगभग दस वर्षों से लंबित थी। दूसरा हवा-पानीपरिवर्तन की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता पर। वह भी इस डर से कि अमेरिका की बागडोर जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं देने वाले ट्रंप के हाथों में जा रही है. इसमें विकासशील देश चाहते थे कि तापमान को मौजूदा स्तर पर लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विकसित देश उन्हें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए सालाना कम से कम 1300 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देना शुरू करें, लेकिन अमीर देश रो रहे हैं सालाना सिर्फ 300 अरब डॉलर देने को तैयार वो भी 2035 से. अमीर देशों का कहना है कि प्रस्तावित राशि मौजूदा 100 अरब डॉलर हैउससे तीन गुना, इसलिए विकासशील देशों को नाराज़ होने के बजाय ख़ुश होना चाहिए, लेकिन विकासशील देशों का कहना है कि यह ज़रूरत का एक चौथाई भी नहीं है. इसीलिए भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे ऊंट के मुंह में तिनका बताया. उन्होंने कहा कि यह समझौता मृगतृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं है. इससे इस गंभीर चुनौती का सामना करने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी.
विकासशील एवं छोटे गरीब देशों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना की। हर साल जलवायु शिखर सम्मेलन में किए गए समझौते और बड़े वादेइसके बावजूद तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पता चलता है कि या तो अब तक उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं या फिर उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा है।
स्टैनफोर्ड में पढ़ाने वाले आर्थिक इतिहासकार वाल्टर डेल की प्रसिद्ध पुस्तक ‘द ग्रेट लेवलर’ के अनुसार, मानव इतिहास में वास्तविक परिवर्तन हमेशा बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के कारण हुए हैं। जलवायु परिवर्तन को बड़े पैमाने पर विनाश की ओर ले जाने से रोकने के लिए ठोस और तीव्र उपाय करने के बजाय हर साल होने वाली अंतहीन बातचीत शीडेल को सही साबित करती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है किजलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सहमति किसी अन्य मुद्दे पर कभी नहीं बन पाई है। इसीलिए बिल गेट्स का मानना है कि हम एक ऐसे युग समझौते पर पहुंच गए हैं जो इतिहास बदल देगा। नई और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बड़ी आपदाओं की रोकथाम हो सकेगी।
सौर, पवन, जल और परमाणु से स्वच्छ ऊर्जा की लागत में तेजी से गिरावट और साथ ही कम ऊर्जा खपत करने वाले वाहनों और मशीनों के विकास के साथ, बिल गेट्स के शब्द विश्वसनीय हैं, लेकिन जयईंधन से चलने वाले वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों को स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली में बदलने के लिए आवश्यक 11,000 अरब डॉलर का निवेश कहां और कैसे आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
बाकू में 2035 से 300 अरब डॉलर की सालाना मदद का वादा किया गया है. क्या तब तक तापमान स्थिर रहेगा? विकसित देशों ने भी विकासशील देशों से आयात पर कार्बन कर लगाना शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ के कार्बन कैप समायोजन तंत्र से भारत जैसे देशों में निर्यातकों के लिए लागत बढ़ जाएगी। इसीलिए विकसित देशबढ़ते तापमान में अपनी भूमिका की याद दिलाते हुए वित्तीय सहायता के लिए दबाव बनाए रखने के अलावा, चीन जैसे विकासशील देशों को जलवायु की रक्षा के लिए स्वयं प्रभावी उपाय करने होंगे। सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश बनने के साथ-साथ चीन स्वच्छ ऊर्जा और उस पर आधारित प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा उत्पादक भी बन गया है। उन्होंने विकसित देशों का मुंह बंद रखने के लिए आर्थिक सहायता में योगदान देने की पहल भी की है. एक तिहाई ग्रीनहाउस गैसें खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और आपूर्ति से जुड़े उद्योगों से आती हैंहो रहे हैं, जिनकी रोकथाम पर गंभीरता से चर्चा तक नहीं हो रही है।
विश्व के जैव ईंधन का लगभग 15 प्रतिशत कृषि और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उत्पादन में खपत होता है। घरेलू पशुओं द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस भी तापमान वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता है। खाद्य प्रसंस्करण, प्रशीतन, पैकेजिंग और आपूर्ति उद्योग भी जैव ईंधन पर चलते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के साथ कृषि चलाने और आयातित खाद्य पदार्थों के बजाय ताजा और मौसमी खाद्य पदार्थों और मांस के बजाय शाकाहार को प्रोत्साहित करने से, लगभग एक तिहाई ग्लोबल वार्मिंग गैसों से बचा जा सकता है।लेकिन विकसित और विकासशील देशों में किसान और खाद्य उद्योग इतने संगठित हैं कि किसी भी सरकार के पास इतने बड़े बदलावों के लिए उन पर दबाव बनाने की इच्छाशक्ति नहीं है।
भारत में इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत हर साल एसिड कोहरे की चादर से ढका रहता है, यह न तो चुनावों में मुख्य मुद्दा बन पाता है और न ही संसद में इस पर कोई सार्थक चर्चा होती है। 1950 के आसपास लंदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI दिल्ली से भी बदतर हुआ करता था। आज दिल्ली की जीडीपी से कई गुना ज्यादा देने के बावजूद लंदन का AQI औसत है20 पर कोई नहीं रहता और दिल्ली 150 पर जो अक्टूबर में 400 को पार कर जाता है।
2013 में बीजिंग का AQI 600 और सिंगापुर का 400 पार कर गया था. आज बीजिंग और सिंगापुर दोनों का AQI दिल्ली से काफी कम है। जनता कमर कस ले तो क्या नहीं हो सकता? सिर्फ सरकारों का मुंह देखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसके कारणों के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। लोगों को पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली आदतों को छोड़ना होगा। पर्यावरण को बनाए रखने के लिएसरकारों द्वारा बनाए गए नियम-कायदों का सख्ती से पालन करना होगा। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जब सरकारी और निजी स्तर पर हर कोई कमर कस लेगा तो स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी।
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार