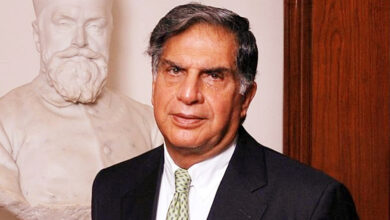अजय कुमार
लखनऊ : भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा के लिए कई कानूनी उपाय और संरक्षण व्यवस्था मौजूद हैं। महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव से बचाने के लिए समाज में जागरूकता और कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी भूमिका निभाते हुए लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने की कोशिश की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अक्सर उठता है कि क्या पुरुषों को अपनी समस्याओं और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का पर्याप्त मंच मिला है? क्या पुरुषों के लिए भी ऐसा कोई आयोग होना चाहिए, जैसा कि महिलाओं के लिए है?
यह सवाल हाल ही में बेंगलुरु के होनहार ए.आई. इंजीनियर, अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद फिर से चर्चा में आया है। अतुल ने घरेलू हिंसा और अपने ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने उनपर झूठे आरोप लगाए, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और सिस्टम से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अतुल की मौत के बाद, इस बात ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत में पुरुषों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता है, जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सके।
भारत में पुरुषों पर अत्याचार के मामलों पर चर्चा करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश पुरुष इन मुद्दों को सार्वजनिक नहीं करते। उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई प्रभावी मंच नहीं होता। आंकड़े भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पुरुषों के आत्महत्या के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 81,063 विवाहित पुरुष थे, जो पारिवारिक समस्याओं, दबाव और घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हुए। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने की क्षमता सीमित होती है, और वे पारिवारिक और घरेलू दबावों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि, घरेलू हिंसा का शिकार होने के बावजूद अधिकांश पुरुष अपनी स्थिति को सार्वजनिक करने में संकोच करते हैं, क्योंकि समाज में पुरुषों के साथ होने वाली हिंसा पर बात करना एक वर्जित विषय बन चुका है
एनसीआरबी और अन्य कई संगठनों के अध्ययन में यह सामने आया है कि पुरुषों को घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि 18 से 49 वर्ष की उम्र की 10% महिलाएं कभी अपने पति पर हाथ उठा चुकी हैं, और 11% महिलाएं पिछले एक साल में अपने पतियों के साथ हिंसा कर चुकी हैं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पुरुषों के खिलाफ हिंसा और मानसिक उत्पीड़न की समस्या को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक और मुद्दा है ये सब खुलकर सामने नहीं आ पाता, क्योंकि पुरुषों को हमेशा यह बताया जाता है कि उन्हें अपनी समस्याओं को छिपाना चाहिए, क्योंकि वे पुरुष हैं और उन्हें मजबूत रहना चाहिए।
भारत में पुरुष आयोग की आवश्यकता को लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले, यह सवाल उठता है कि क्या पुरुषों को भी महिलाओं के समान अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त कानून हैं, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग कभी-कभी पुरुषों के खिलाफ भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, दहेज उत्पीड़न के मामलों में झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए कोई मंच नहीं है, जहां वे अपनी बात रख सकें और न्याय पा सकें। खासतौर पर, धारा 498A (दहेज उत्पीड़न कानून) का कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत पुरुषों को और उनके परिवार के सदस्यों को झूठे आरोपों के तहत फंसाया जाता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कई बार चेतावनी दी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामलों की संख्या कम नहीं हो रही है।
पुरुष आयोग का गठन इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे पुरुषों को अपनी बात रखने का एक मंच मिलेगा। यह आयोग पुरुषों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक हिंसा के मामलों में न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह आयोग दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य कर सकता है। अगर महिलाओं के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है, तो पुरुषों के लिए भी समान रूप से एक आयोग होना चाहिए, जिससे उनके मुद्दों को सही तरीके से उठाया जा सके।
पुरुष आयोग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों के लिए दिशा-निर्देश देने और एक आयोग बनाने की अपील की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इसमें एकतरफा तस्वीर पेश की गई है। अदालत ने यह तर्क दिया कि पुरुषों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले उतने अधिक नहीं हैं, जितने महिलाओं के खिलाफ होते हैं, और इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कई लोगों के लिए निराशाजनक था, क्योंकि यह दर्शाता है कि पुरुषों के उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस विचारधारा को मजबूत करता है कि हमारे समाज में पुरुषों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को बहुत हलके में लिया जाता है। अगर पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई समिति या आयोग नहीं है, तो इसका मतलब है कि समाज को यह स्वीकार करना चाहिए कि पुरुषों के लिए कोई गंभीर समस्या नहीं है। यह मानसिकता भी समाज में बदलाव की जरूरत को दिखाती है।
यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा बढ़ रही है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में 2022-2023 के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू हिंसा के 3 पीड़ितों में से एक पुरुष है। अमेरिका में लगभग 44% पुरुष अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार हिंसा का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा, मेक्सिको में घरेलू हिंसा के पीड़ितों में करीब 25% पुरुष होते हैं। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पुरुषों के खिलाफ हिंसा की समस्या वैश्विक है, और इसके लिए भी कानूनी उपायों की आवश्यकता है।
अतुल सुभाष की आत्महत्या ने न केवल भारत में पुरुषों के अधिकारों के मुद्दे को उजागर किया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या हमारे न्यायिक और पुलिस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा था कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो उसकी अस्थियों को कोर्ट के सामने नाले में डाल दिया जाए। यह एक गहरी निराशा और सिस्टम से विश्वास की कमी को दर्शाता है। अतुल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए थे, लेकिन उनका असली गुस्सा सिस्टम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ था, जिन्होंने उनके मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। अतुल की आत्महत्या को लेकर मीडिया और समाज की प्रतिक्रिया बहुत ही विभाजित रही है, और कई लोग इसे पुरुषों के उत्पीड़न का एक उदाहरण मानते हैं।
अतुल सुभाष की मौत की घटना हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारे समाज और न्याय व्यवस्था को किस प्रकार सुधारने की आवश्यकता है। यह सवाल केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव का नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम का मुद्दा है जो उन सभी पीड़ितों के लिए काम नहीं करता जो न्याय की उम्मीद में जीते हैं। अतुल की आत्महत्या ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिस्टम की खामियों और न्याय की कमी की वजह से कई लोग अपनी जान गवा देते हैं। हमें अपने न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिल सके।
अतुल सुभाष की मौत, उनके आरोप और उनके द्वारा उठाए गए सवाल हमारे समाज और कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि पुरुषों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महिलाओं की है। समाज में मानसिकता बदलने और कानून के उचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने उत्पीड़न और दर्द को चुपचाप न सहन करे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में समानता हो, तो हमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के अधिकारों की रक्षा एक समान तरीके से करनी होगी।